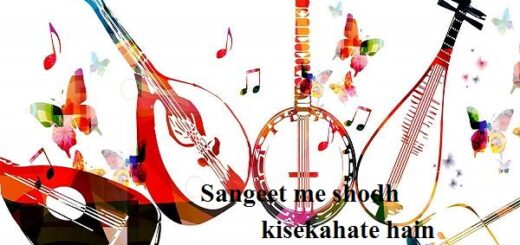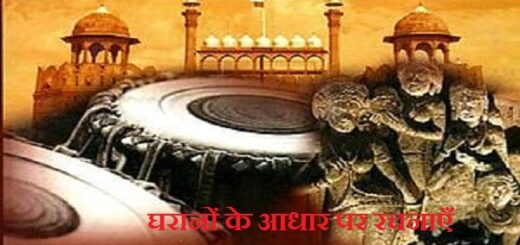राग परिवार (रागंग) और मिश्रित राग (जोड़ राग) || Raga Parivar (Ragang) and Mixed Raga (Jod Raga)|| गंभीर रागों का परिचय ||
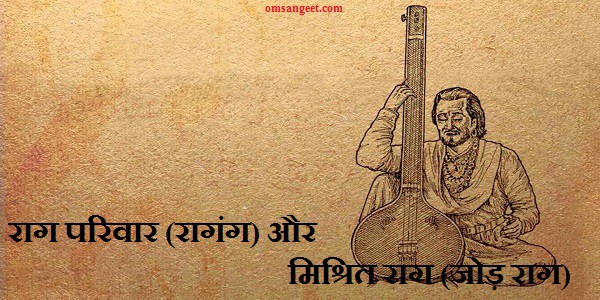
गंभीर रागों का परिचय
राग परिवार (रागंग) और मिश्रित राग (जोड़ राग)
Raga Parivar (Ragang) and Mixed Raga(Jod Raga)
यह पृष्ठ भारतीय शास्त्रीय संगीत में कुछ अधिक वजनदार रागों के माध्यम से राग परिवारों की अवधारणा की पड़ताल करता है – मलकौंस, दरबारी कनाडा, मिया मल्हार, और उनकी शाखाएं – चंद्रकौंस, संपूर्ण मालकौन्स, कौंसी कनाडा और मेघ।
राग परिवार (रागंग) तब बनते हैं जब नए राग मौजूदा रागों से प्राप्त होते हैं। एक मौजूदा राग लें और उसके पैमाने से एक नोट छोड़ दें, और आपके पास एक नया राग है। एक नया नोट जोड़ें, और आपके पास एक अलग राग है। आप राग के आरोही पैमाने में या केवल विशिष्ट नोट पैटर्न में चुनिंदा रूप से नोट्स छोड़ सकते हैं या जोड़ सकते हैं। एक ही परिवार के रागों के माधुर्य प्रोफाइल या चलन (वीडियो: “क्या चलन है?”) अक्सर समान होते हैं।
उदाहरण के लिए राग मालकौन्स को ही लें। यह सा गा मा धा नी (1, ♭3, 4, 6, 7) नोट्स का उपयोग करता है। यदि आप नी को नी से प्रतिस्थापित करते हैं, तो आपको राग चंद्रकौं (सा गा मा ध नी; 1, 3, 4, 6, 7) मिलते हैं। यदि आप मालकौन्स लेते हैं और उसमें दो नोट, रे और पा मिलाते हैं, तो आपको राग संपूर्ण मालकौन्स (सा रे गा मा पा धा नी; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) मिलता है। तीनों राग कौन्स परिवार से संबंधित हैं और नोटों के समान पैटर्न का उपयोग करते हैं। इस बीच, राग दरबारी कनाडा संपूर्ण मालकौन्स(सा रे गा मा पा धा नी; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) के रूप में नोट्स के एक ही सेट का उपयोग करता है, लेकिन इसकी माधुर्य प्रोफ़ाइल अलग है क्योंकि इसमें है एक अलग मूल। यह कनाडा परिवार से संबंधित है। आइए एक राग से दूसरे राग की प्रगति पर एक नज़र डालें कि यह व्यवहार में कैसे काम करता है।
राग मालकौन्स (कौन्स अंग)
मालकौन्स एक प्राचीन राग है और हिंदुस्तानी (उत्तर भारतीय) और कर्नाटक (दक्षिण भारतीय) शास्त्रीय संगीत दोनों में बहुत महत्वपूर्ण है। यह विशाल और गहरा है, निचली पिच रेंज में सबसे अच्छा प्रदर्शन सुबह के छोटे घंटों में, मध्यरात्रि के ठीक बाद बेहद चिंतनशील गति से किया जाता है।
राग चंद्रकौंस (कौन्स अंग)
इतने सारे सपाट नोटों का उपयोग करने के बावजूद, इसके नोटों की एक समान दूरी के कारण मालकौन्स में कोई अंधेरा नहीं है। लेकिन फ्लैट नी (♭7) को नी (7) से बदलें, और आप तुरंत पैमाने पर तनाव और अंधेरे का एक तत्व जोड़ते हैं। चंद्रकौंस एक नया राग है, जो मालकौंस से निर्मित है। मालकौन्स की तरह ही यह आधी रात के बाद किया जाता है।
राग संपूर्ण मालकौन्स (कौन्स अंग)
मेरे लिए संपूर्ण मालकौन्स , मालकौन्स का अधिक स्त्री संस्करण है। यह अपेक्षाकृत नया राग भी है और दुर्लभ भी। यह ज्यादातर जयपुर-अतरौली घराने (स्कूल) के कलाकारों द्वारा किया जाता है। एक बार फिर इस राग के लिए निर्धारित समय मध्यरात्रि के बाद का है।
राग मिया मल्हार (मल्हार अंग)
और अब मल्हार रागों में सबसे प्रसिद्ध मिया मल्हार की एक झलक के लिए। मिया मल्हार की लोकप्रियता फिल्मी गीतों सहित हल्की शैलियों में इसके विपुल उपयोग के कारण है, जहां इसे तदनुसार अधिक हल्के ढंग से व्यवहार किया जाता है। मुख्यधारा के शास्त्रीय संगीत में, हालांकि, कठिन माइक्रोटोन और भारी दोलनों के उपयोग के कारण इसे मास्टर करना एक अत्यंत कठिन राग माना जाता है। इसके वाक्यांशों की घुमावदार (वक्र) प्रकृति भी इस राग में बड़े पैमाने पर सुधार करने के लिए काफी चुनौती देती है, हालांकि स्पष्ट रूप से अद्वितीय भीमसेन जोशी के लिए नहीं।
गंभीर रागों का परिचय
राग बागेश्र्वरी
| थाट | काफी |
| जाति | ओड़व – सम्पूर्ण |
| वादी | म |
| सम्वादी | सा |
| स्वर | ग ,नि कोमल शेष शुद्ध |
| वर्जित स्वर | आरोह में रे प |
| समय | रात्रि का दूसरा प्रहर |
यह एक गंभीर प्रकृति का राग है मधुर एक मधुर और कर्णप्रिय राग होने के कारण उप शास्त्रीय संगीत शैली में और सुगम संगीत में इसकी अनेक बंदिशें देखने को मिलती है बागेश्वरी में धनश्री और कान्हड़ा का योग माना जाता हैं इस राग की जाति के विषय में विद्वानों में मतभेद पाया जाता हैं इसका चलन तीनों सप्तकों में समान रूप से होता है। ग्रंथों में इसका सम प्राकृतिक राग श्रीरंजनी को बताया जाता है।
राग बिहाग परिचय
आरोहन में रे ध वर्जित, गावत राग बिहाग ।
प्रथम प्रहर निशी गाइये, सोहत ग-नि सम्वाद ।।
| थाट | बिलावल |
| जाती | औड़व-सम्पूर्ण |
| वर्जित स्वर | आरोह में रे और ध |
| वादी | गांधार |
| समवादी | निषाद |
| गायन समय | रात्रि का दूसरा प्रहर |
| लगने वाले स्वर सभी शुद्ध स्वर, तीव्र मध्यम का अल्प प्रयोग |
इस राग की रचना बिलावल ठाठ से मानी गई है।इस राग के आरोह में रे ध स्वर वर्जित और अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किये गाए हैं इसलिए इसकी जाती औडव-सम्पूर्ण है। इसे रात्रि के प्रथम प्रहर के मध्य भाग में गाया बजाया जाता है। वादी स्वर गंधार और समवादी स्वर निषाद है।यह पूर्वांग प्रधानराग है इसलिए इसका चलन मंद्र और मध्य सप्तक में अधिक पाया जाता है। इस राग का आरोह-अवरोह इस प्रकार है-
| आरोह | नि सा ग म प नि सां। |
| अवरोह | सां नि ध प म ग रे सा । |
| पकड़ | नि़ सा ग म प, म॑ प ग म ग, रे नि़ सा। |
| स्वरूप | गमग रेसा, निसांनि नि-प, निधप पम॑ग म, ग म ग- रे नि़ सा। |
इसका ग्रह स्वर निषाद है क्योंकि इसका चलन मंद्र नि से प्रारम्भ किया जाता है जैसे- नि सा ग म प । आरोह में रिषभ और धैवत वर्जित है, किन्तु अवरोह में इनका अल्प प्रयोग है अथवा यह दुर्बल और अनुगामी माने गये है। ज़्यादातर इन्हें कण स्वर के रूप में अवरोह में प्रयोग करते है, जैसे- सां नि s धप, ध प गम ग s रेसा । यदि यह स्वर प्रबल हो जाएँगे तो इसमें राग बिलावल की छाया आने लगेगी। इसकी प्रकृति गंभीर मानी गयी है इसलिए इसमें विलंबित ख्याल, द्रुत ख्याल तथा तराना गाया जाता है। इसमें गंधार वादी स्वर के साथ अंश स्वर और न्यास-बहुत्व स्वर भी है। जैसे- नि़ सा ग, ग म प ग म ग, प म॑ ग, म ग s सा। राग की सुंदरता और रंजकता बढ़ाने के लिए कभी-कभी अवरोह में तीव्र मध्यम का प्रयोग पंचम के साथ विवादी स्वर की तरह किया जाता है, जैसे- प म॑ ग म ग, रेसा। आजकल तीव्र मध्यम प्रयोग इतना अधिक बढ़ गया है की इसे राग का आवश्यक स्वर माना जाने लगा है। इसका अधिक प्रयोग होने से कुछ लोग इसे कल्याण ठाठ का राग मानने लगे है। कुछ गायक बिहाग में तीव्र म का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते और उसे शुद्ध बिहाग कहते हैं।कुछ कलाकारों का मानना है की आलाप करते समय तीव्र मध्यम और मंद्र निषाद पर मंद आवाज़ से न्यास किया जाए तो निराशा और हृदय में संवेदना उत्पन्न होगी।यह एक शुद्ध राग है क्योंकि इसमें किसी दूसरे राग की छाया या मिश्रण नहीं है। इसके अन्य प्रकार है- बिहागड़ा, नटबिहाग, मारूबिहाग, पटबिहाग, आदि।